जनपद चमोली में रिंगाल हस्तशिल्प एवं आगाज़ के प्रयास- एक दृश्यावलोकन
- AAGAAS FEDERATION
- Sep 21, 2024
- 6 min read
उत्तराखण्ड का सीमान्त जनपद चमोली पूर्व से ही संस्कृति, परम्पराओं और स्थानीय स्तर पर प्रचलित हस्तशिल्प कलाओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ प्रचलित हस्तशिल्प कलाओं में ऊनी वस्त्र निर्माण, कालीन एवं मूर्तिकला, तांबे के बर्तन, लौह शिल्प कला के साथ-2 स्थानीय संसाधन आधारित रिंगाल हस्तशिल्प कला भी जाना जाता है। पूर्व में भारत चीन तिब्बत व्यापार के 1962 से पूर्व नीति मलारी माणा घाटियों से सतत् जारी रहने के परिणामस्वरूप या ऊन के अत्यधिक उत्पादन के साथ-2 सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत् भोटिया जनजाति समुदाय के द्वारा ऊनी वस्त्र निर्माण एवं ऊन और रेशे आधारित हस्तशिल्प के उत्पादन खूब प्रचलन में थे।
दूसरी तरफ पहाड़ी समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पिछडे़ अनुसूचित जाति जिसमें औजी, लौहार, टम्टा, धौसिया, राजमिस्त्री, बाडै, तेली, कोली और रिंगाल का कार्य करने वाले रूडिया वर्ग के लोग थे। जिन्हें उनके आजीविकावर्धन हेतु किये जा रहे कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। सम्भवतः इनका सामाजिक वितरण/ विभाजन इसके द्वारा जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में लाये जा रहे प्राकृतिक संसाधन और उनके द्वारा बनाये गये उत्पादों पर निर्भर करता रहा होगा। उदाहरण के लिए औजी लोग ढोल-दमाऊ जैसे वाद्य यंत्र बजाते थे इसलिए उन्हें औजी, स्थानीय फसलों और अनाजों से पुरातन रजवाडे प्रथाओं के दौरान हस्तचालित कोल्हू जिसमें शारीरिक श्रम बहुत अधिक लगता है से तेल निकालने वाले वर्ग को कोली, तांबे के बर्तन बनाने वालो को लौहार कहते थे और जंगलो में मौजूद प्राकृतिक संसाधन रिंगाल का उपयोग कर हाथ से बनायी जाने वाली वस्तुएं जो प्रमुखतः खेती के उपयोग में आती थी, बनाने वाले अनुसूचित जाति वर्ग को रूडिया के नाम से जाना जाने लगा।
हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों मे जब गाँव बसे हांेगे तो मनुष्य ने रहन-सहन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए खेती वाली जगह पर बसना पसन्द किया जहाँ पर्याप्त मात्रा में जंगल, पानी और कृषि हेतु भूमि उपलब्ध थी। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अधिकतर मैदानी क्षेत्रों से सदियों पूर्व आकर बसे हैं। जिसके कई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। गाँव पहले छोटे-छोटे थे और ताकतवर और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न गाँवों के आस-पास जीविकोपार्जन और रोजगार प्राप्त करने हेतु अलग-अलग कार्यों में दक्ष लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछडे़ अन्य वर्गों जैसे अनुसूचित जाति के लोग जा आकर बसने लगे। वे आस-पास के गाँव के निवासियों को उनकी आवश्यकतानुसार उपयोग में आने वाली वस्तुएं बनाकर उपलब्ध कराने लगे यह व्यापार पैसे के स्थान पर वस्तु-विनिमय पर आधारित होता था।
इनमें रिंगाल का कार्य करने वाले अनुसूचित जाति के रूडिया भी शामिल थे जो गाँवों के सम्पन्न वर्ग को अनाज, आभूषण, चारा तथा अन्य कृषि कार्य हेतु रिंगाल की बनी वस्तुयें उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार रूडिया वर्ग गाँव की सामाजिक और पारिस्थितिकीय तंत्र का हिस्सा बनकर गाँव के ढाँचे में उपेक्षित लेकिन महत्वपूर्ण अंग के रूप में बसने लगा। गाँव से रूडिया वर्ग की आजीविका चलने लगी तब रोजगार की बजाय जीविकोपार्जन ही महत्वपूर्ण बिन्दु हुआ करता था।
रूडिया समुदाय- एक परिचय
पहाड़ के सामाजिक ढाँचें में आज भी जातियों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। जाति एवं कार्य के आधार पर गाँव का आर्थिक विभाजन देखने को मिलता है और आर्थिक तथा शैक्षणिक विभाजन के आधार पर यह भी महसूस किया जाता रहा है कि इनके मध्य सामूहिक एकता का अभाव हैं अपने-अपने स्वार्थों के लिए सत्ता पक्ष एवं दबंग समुदायों द्वारा इनका समय-समय पर शोषण किया जाता रहा है। शिक्षा का स्तर अच्छा न होना, महिला साक्षरता के प्रतिशत में कमी, समाज में उपेक्षित स्थान पर होने के कारण यह समुदाय वर्तमान आवश्यकताओं और परिदृश्य के अनुरूप प्रगति नहीं कर पाता है। इसके लिए जहाँ सरकारी/गैर सरकारी विभाग और योजनायें जिम्मेदार हैं वहीं इस समुदाय के लोग भी स्वयं कम जिम्मेदार नहीं माने जा सकते हैं। सामाजिक उत्प्रेरण का समुदाय में अभाव है।
रिंगाल व्यवसाय उत्तराखण्ड की दलित समुदाय के एक विशेष वर्ग, जिन्हें स्थानीय भाषा में कुमाऊं क्षेत्र में बेडी तथा गढवाल क्षेत्र में रूडी कहा जाता है, के जीविकोपार्जन से सदियांे से जुड़ा रहा है। प्राचीन काल से ही यह पहाड़ी क्षेत्र का प्रमुख कुटीर उद्योग रहा है। विशेषतया गढवाल में एक जाति विशेष (रूडिया) का यह परम्परागत रूप से जीविका का साधन रहा है। ये लोग आज भी रिंगाल से बनायी गयी वस्तुओं को पीठ पर लाद कर गाँवों और कस्बांे में बेचने जाते हैं। इस व्यवसाय को उत्तराखण्ड में बहुत महत्व पूर्ण माना जाता रहा है, और यही कारण है कि आज बदलती हुई परिस्थितियांे में भी यह उद्यम जीवित है। दूरस्थ गाँवों तक भले ही प्लास्टिक और पाॅलिथीन के आकर्षक बर्तन या उपकरण पहँुच गये हों लेकिन रिंगाल शिल्प ने आज भी अपना स्थान गाँव से लेकर महानगरों तक बरकरार रखा है। अच्छे और आकर्षक रिंगाल शिल्प की मांग दिनों दिन बढती जा रही है। इससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में जहाँ एक और रिगाल शिल्प को प्रोत्साहन मिलेगा वहीं दूसरी तरफ जंगलों में कच्चे माल की कमी भी होने लगेगी। क्योंकि अभी तक रिगाल को सामूहिक वन पंचायत, बेकार भूमि पर उगाने या कृषि करण के प्रयास शुरू नहीं हो पाये हैं। और रूडीया समुदाय इसे मुफ्त संसाधन मानते हुए इस कच्चे माल का कोई मूल्य आंकलित नहीं करता है। यही नहीं सामूहिक रूप से इस समुदाय द्वारा जंगलो में या जंगल के बाहर अलग-अलग प्रजाति के रिंगाल को संरक्षित रखने और भविष्य में कच्चे माल के रूप में उसे उपयोग करने, नर्सरी विकास या वनीकरण के प्रयास नहीं किये गये हैं। इससे पर्यावरणविदांे औार वनस्पतिशास्त्रियों के मन में चिंता है कि रिंगाल को मुफ्त का संसाधन मानकर बेतरतीब और अवैज्ञानिक तरीके से जंगलों से काटकर लाया जा रहा है। लेकिन समुदाय या सरकारी/गैर सरकारी प्रयासों से रिंगाल संरक्षण एवं उत्पादन के प्रयास अभी तक मूर्त रूप नहीं ले पाये है।
सामान्यतः रूडिया जाति के लोग लौहार और औजी की तरह गाँव के सामाजिक ढाँचे का महत्वपूर्ण अंग है। और गाँव में एक विशिष्ट स्थान भी रखते हंै। हालांकि यह वर्ग अनुसूचित जाति के लोगों की ही तरह वर्तमान समय में भी गरीब, शोषित और उपेक्षित है। आरक्षण की नीतियां भी उसके सामाजिक, आर्थिक विकास हेतु पर्याप्त साबित नहीं हुई। क्यांेकि साक्षरता का स्तर तो ठीक-ठाक है लेकिन उच्च शिक्षा के अवसर बेहद क्षीण है। इसके लिए प्रमुखतः अच्छी कृषि भूमि का अभाव (अधिकतर भूमिहीन) परिवार में सदस्यों की अधिकता, सामाजिक जागरूकता का अभाव, उच्च शिक्षा के प्रति रूझान में कमी, राजनैतिक प्रतिनिधित्व का अभाव और महिला वर्ग के लिए उपेक्षा भी अन्य कारकों में प्रमुख है, इसमंे बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदासीनता है।
रूडिया समुदाय के लोग प्राचीन समय से ही रिंगााल के उत्पादन बनाते रहे हैं। इस हस्तशिल्प कला की वजह से गाँव के संभ्रान्त वर्ग व समाज की उपेक्षित रूडिया वर्ग के बीच सामाजिक सम्बन्ध रहा है। यहाँ यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि हस्तशिल्प कला की उपयोगिता सुन्दरता और महत्व के कारण ही रूडिया समुदाय गाँव के सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग माने जाते रहे हंै।
इस कार्य के लिए अधिक औजारों उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही इसमंे ज्यादा पेंचीदगी है। प्रमुखतः दरांती एवं चाकू ही प्रयुक्त होेते हंै। रिंगाल की छड़ों को वस्तुएं बनाने हेतु कूटकर व छीलकर सपाट किया जाता है। इस कार्य को जितनी दक्षता एवं कलात्मक ढंग से किया जाता है, उतना ही बनायी गयी वस्तु में निखार व आकर्षण आता है। परम्परागत रूप से ग्रामीण रिंगाल की बनी वस्तुओं का प्रयोग अनाज रखने, सुखाने, सामान ढोने एवं अन्य रूपों में किया करते है। परम्परागत रूप से उपयोग में आने वाली वस्तुएं, कण्डी, सूप, टोकरियां चटाईयां आदि है।
जनपद चमोली में रूडिया समुदाय की बसावट का सर्वेक्षण करने पर यह तथ्य सामने आये हंै कि ज्यादातर ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ सदाबहार वनों की अधिकता है उन्हीं गाॅवों के आस पास रिगाल हस्तशिल्प का कार्य अधिक होता है। यही नही ऊॅचाई वाले क्षेत्रों जैसे जोशीमठ विकास खण्ड के - लाता, रिगी, करछौं, करछी, तुगासी, थैग, सलूड, डुगरा, डुमक, कल्गोठ, सलना, उर्गम, मोल्टा, पगनौ, गणाई, पाखी, टंगणी, दाडमी गाँवों में रूडिया लोग निवास करते हैं और अधिकतर गाँव के ही उपयोग में आने वाले रिंगाल उत्पाद बनाते है। यही नहीं इन गाँवो के सामान्य वर्ग के ग्रामीण भी अपने स्वयं के उपयोग के लिए मोटी बुनाई वाले उत्पाद जैसे कण्डी, चंगेरा आदि बनाते हैं, परन्तु ये इन्हंे बाजारो में बेचने के लिए नहीं बनाते। दूसरी तरफ सड़कांे के निकट बसे गाँवों - पाखी, टगणी के रूडिया लोग नये आकर्षक छोटे उत्पाद बनाते हैं, जिसको वे तीर्थयात्रियों व पर्यटकों को बेचते हैं। लेकिन ये विपणन का कार्य समूहों द्वारा स्वयं नहीं किया जाता है।
रिंगाल एक दृश्यावलोकन
पहाड़ की अर्थव्यवस्था के साथ रिंगाल का अटूट रिश्ता रहा है। रिंगाल बांस की तरह की ही एक झाड़ी है। इसमें छड़ी की तरह लम्बे तने पर लम्बी एवं पतली पत्तियां गुच्छी के रूप में निकलती है। यह झाड़ी पहाड़ की संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण वनस्पति समझी जाती है। पहाड़ के जनजीवन का पर्याय रिंगाल, पहाड़ की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ अंग रहा है। प्राचीन काल से ही यहाँ के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का श्री गणेश रिंगाल की बनी कलम से होता था। घास लाने की कण्डी से लेकर सूप, टोकरियां, चटाईयां, कण्डे, बच्चों की कलम, गौशाला, झोपडी तथा मकान तक में रिंगाल अनिवार्य रूप में लगाया जाता है। और अधिक जानकारी और रिंगाल के बारे में विस्तृत रूप से पढ़िए आगे लिखे लेख में -





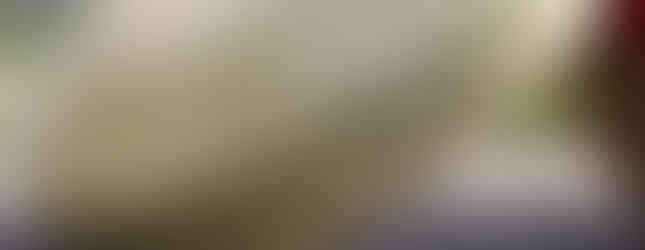




















Comments